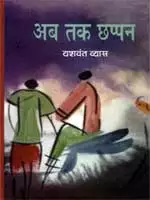|
हास्य-व्यंग्य >> अब तक छप्पन अब तक छप्पनयशवंत व्यास
|
27 पाठक हैं |
|||||||
‘अब तक छप्पन’ के व्यंग्य दिलचस्प अन्दाज़ तथा विश्वसनीय प्रहार-क्षमता से आपको उस जगह खड़ा करते हैं जहाँ से आप सच को सच की तरह देख सकें।
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
यशवंत व्यास को नयी पीढ़ी के रचनाकारों में भाषा और शिल्प के स्वर पर
अद्भुद ताज़गी के लिए जाना जाता है। ‘अब तक छप्पन’
में उनकी
चुनी हुई व्यंग्य रचनाएँ है। रचनाओं की विषयवस्तु और मुहावरे दोनों ही
सत्तर के दशक के बाद बनते-बिगड़ते संसार की प्रतिध्वनि हैं। सामाजिक
सरोकारों, बाजारवादी प्रभावों तथा मीडिया के जरिये सूचना क्रांति के
नतीजों पर मार्मिक टिप्पणी इनमें देखी जा सकती है।
हास्य की हा-हाकारी परम्परा से उलट, यशवंत के व्यंग्य में तीव्र वेदना का स्वर है। उनकी शैली में पारम्परिक हास्य-बोध की शाब्दिक बाजीगरी न होकर स्वरूप का गहन संसार पाठकों को व्यंग्य के नये अनुभव प्रदान करता है। उनके मुहावरे अपने समय के द्वारा निर्मित हैं, प्रयोगशीलता जिन्हें कई बार नये समय की सूक्तियों बदल देती है।
प्रतिबद्धता यशवंत सिंह की रचनाओं की बड़ी विशेषता है। धिक्कार की राजनीति में प्रवीण चरित्रों के वैचारिक जगत की पड़ताल इसके माध्यम से की जा सकती है। सहजता और चमत्कारिकता इन रचनाओं का अन्तनिर्हित गुण है, किन्तु यह भाव भूति के सार्थक विस्तार में प्रयुक्त होता जाता है। विषय नये हैं शैली ऊबाऊपन और रूढ़ियों से दूर है और पठनीयता इनका अनिवार्य तत्त्व है।
‘अब तक छप्पन’ के व्यंग्य दिलचस्प अन्दाज़ तथा विश्वसनीय प्रहार-क्षमता से आपको उस जगह खड़ा करते हैं जहाँ से आप सच को सच की तरह देख सकें।
हास्य की हा-हाकारी परम्परा से उलट, यशवंत के व्यंग्य में तीव्र वेदना का स्वर है। उनकी शैली में पारम्परिक हास्य-बोध की शाब्दिक बाजीगरी न होकर स्वरूप का गहन संसार पाठकों को व्यंग्य के नये अनुभव प्रदान करता है। उनके मुहावरे अपने समय के द्वारा निर्मित हैं, प्रयोगशीलता जिन्हें कई बार नये समय की सूक्तियों बदल देती है।
प्रतिबद्धता यशवंत सिंह की रचनाओं की बड़ी विशेषता है। धिक्कार की राजनीति में प्रवीण चरित्रों के वैचारिक जगत की पड़ताल इसके माध्यम से की जा सकती है। सहजता और चमत्कारिकता इन रचनाओं का अन्तनिर्हित गुण है, किन्तु यह भाव भूति के सार्थक विस्तार में प्रयुक्त होता जाता है। विषय नये हैं शैली ऊबाऊपन और रूढ़ियों से दूर है और पठनीयता इनका अनिवार्य तत्त्व है।
‘अब तक छप्पन’ के व्यंग्य दिलचस्प अन्दाज़ तथा विश्वसनीय प्रहार-क्षमता से आपको उस जगह खड़ा करते हैं जहाँ से आप सच को सच की तरह देख सकें।
कथन
मुझे यूटोपिया का पता नहीं था। शुरू-शुरू में मुझे यह किसी ऐसे विदेशी
शब्द का अहसास कराता जिसे अमूमन कुछ ‘दादा’
मार्क्सवादी मजाक
का मामला समझते थे। पर इस शब्द में कोई ऐसी शक्ति जरूर थी जो उसे उसके
खिलाफ आलोचना के केन्द्र में ला रही थी। कोई आदर्श बात कहते ही, अंग्रेजी
के वाक्य तथा विदेशी नाम टपकाने में माहिर एक अग्रज चिढ़ते हुए घोषित करते
कि ‘यह महज यूटोपिया’ है। बाद में पता चला यह एक
स्वप्निल
काल्पनिक आदर्श दुनिया का सन्दर्भ है। बताया गया कि बर्तानवी रचनाकार
थॉ़मस मूर ‘यूटोपिया’ लिखा था, जिसमें ऐसा आदर्श समाज
था जो
न्याय और विवेक से ही चलता था। इसी वजह से हर आदर्श समाज की कल्पना
यूटोपिया कही जाने लगी थी। जब यह मान लिया गया कि आदर्श समाज नाम की चीज
व्यावहारिक जीवन में असम्भव है तब यूटोपिया मजाक हो गया।
मुझे हर मजाक में कोई प्यारी चीज नजर आती थी। जैसे भटकटैया के फूल खिले हों तो भी मैं मोगरे वगरैह की सोच सकता था। मोगरी से कपड़े कूटने की ध्वनि में मुझे, धोबियों की छुट्टी कौन से दिन होगी-यह विचार परेशान करता था। उम्र का दोष था। सपने देखते थे और पागल होने की प्रतिष्ठा समझते थे। विवेक और न्याय के सहारे भाषण बेहतर बन जाते थे और पुरस्कार देनेवाले वे सर्वगुण सम्पन्न सेठजी निकलते जो एक सरकारी मान्यता प्राप्त और दूसरी गैर-मान्यता प्राप्त सेठानी रखे हुए लोगों को पूरे मन से उपदेश देते थे। इस तरह यूटोपिया की टोपियाँ उछलती रहती थीं।
डर बढ़े, चेतावनियाँ बढ़ीं, पर सपने देखना नहीं छूटा।
मैं अभी भी मैटिनी शो तक के सपने बदस्तूर देखता हूँ। मैंने पहला उपन्यास लिखा था तो उसकी भूमिका में कहा-
कहते हैं सपनों में कोई क्रम नहीं होता। पात्र भी कभी बबूल होते हुए आम हो जाते हैं, कभी आम होते हुए बबूल। कभी खंडहर, साँप, चोर, उड़ान आपस में जा मिलते हैं। कुछ लोग सपने में रोते हैं, दाँत किटकिटाते हैं, घबरा जाते हैं, चीख पड़ते हैं, उठ जाते हैं, मुस्कुराते हैं या सुबह होने पर लगभग उसे भूल भी जाते हैं। पर, कुछ-बुरे कुछे-अच्छे स्वप्न जब भी आते हैं-याद रह जाते हैं। इनकी अर्थहीनता में भी एक अर्थ होता है और भंग-अंग के बावजूद एक क्रम। अवचेतन तक पहुँचने का यह जादुई रास्ता, ‘स्वप्नविचार’ की पारम्परिक पुस्तिकाओं की व्याख्याओं से ऊपर जाकर एक यात्रा पर ले जाता है। कुछ इससे गुत्थियाँ भी खोल लेते हैं, कुछ इसके दोष से घबराकर हकीमों के पास चले जाते हैं। बावजूद इसके हर आदमी को सपने बगैर कहे आते हैं, और एक यात्रा पर ले जाते हैं। कभी दो किलोमीटर तो कभी दो लाख किलोमीटर भी। हम इन्हें आपस में मिलाये बगैर इनमें सामंजस्य ढूँढ़ने और सुख तथा दुःख की अण्टी मारे बिना रह भी नहीं सकते।
सपनों के साथ यह दिक्कत है कि हम तय करके उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन उतनी ही सुविधा यह है कि उन्हें देखने पर चाहें तो अपने-अपने अर्थ जरूर निकाल सकते हैं।
कहते हैं, जब एक सपने में साँप ने मुँह में पूँछले ली तो उससे कैकुले को कार्बनिक रसायन की बेंजीन रिंग का सूत्र मिल गया था। यानी सपने का अर्थ किसी को जम जाए तो कार्बनिक रसायन का सूत्रपात भी हो जाता है लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि हर सूत्र सपने से उपजता है।
मैं बुरी तरह सपने देखता हूँ। चूँकि सपने देखना न देखना अपने बस में नहीं होता, मैंने भी इन्हें देखा। आप सबकी तरह मैंने भी कभी नहीं चाहा कि स्वप्न, फ्रायड या युंग जैसों की सैद्धान्तिकता से आक्रान्त होकर आएँ या प्रसव पीड़ा की नीम बेहोशी में अखिल विश्व के पाप निवारक ईश्वर के अवतार की सुखद आकाशवाणी के प्ले-बैक के साथ।
सपनों की प्रकृति के अनुरूप भयंकर रूप से एक-दूसरे में गुमे हुए काल, स्थान और पात्रों के साथ मैंने अपने सपनों की यथासम्भव जमावट का एक चालू चिट्ठा पेश किया और ऊपर से कहा-‘यदि तावदयं स्वप्नों धन्यमप्रतिबोधनम्।’ जैसा कि भास की ‘स्वप्नवासवदत्ता’ में आता है-यदि यह स्वप्न है, तो न जागना ही अच्छा होता।
मेरा सपना, इस लिहाज से छुपा हुआ नहीं है। आदर्श मुझे खींचता है, बनाता है, पैमाना रखता है, एक तलाश के लिए प्रवृत्त करता है। हर आदमी को रोटी, कपड़ा मकान दिये जाने का स्टीरियोटाइप क्रान्तिवादी सपना आजकल कवि के उस गेटअप की तरह है जिसे फटे कुर्ते, बढ़े बाल और झोले के सहारे स्थायी मान लिया गया है। मैं अपने सपने में इस चालूपन का प्रतिकार करता हूँ, कभी-कभी इसीलिए बहुत बुरे सपने भी आते हैं।
मैं स्वनामधन्य कलावादी की तरह चाँद पर बैठकर धरती को देखता हूँ तो एक मनुष्य की स्थिति समूची पृथ्वी के मुकाबले चींटी से भी गयी-बीती नजर आती है। पर, यह देखने के लिए चाँद पर जाना जरूरी है। यह भी तभी होगा जब वही मनुष्य चाँद पर जाने लायक वैज्ञानिक इन्तजाम करे। इसलिए आदर्श समाज और नैतिक आस्थाएँ मुझे शक्ति देती हैं। करुणा और प्रेम सपने की ईंट-सीमेण्ट बन जाते हैं। पर, सच्चे जीवन के लिए वैज्ञानिक तर्कवाद चाहिए।
हर व्यक्तिगत स्वप्न, दूसरे के स्वप्न में हस्तक्षेप के साथ बनता है। जैसे पाँच सितारा होटल में शानदार दावत का स्वप्न, वेटर के उस स्वप्न पर चढ़ा मिलेगा जिसमें वह वेटर दावत से मिली टिप के पैसे गिनते हुए अपने पिता की दवाई का ध्यान करेगा। लेकिन, शायद आदर्श समाज सपनों में हस्तक्षेप की बजाय सपनों में साझे से शक्ति लेता होगा। इसलिए ‘कौन बनेगा करोड़पति का स्वप्निल झाँसा, ‘कौन करेगा करोड़ों का कल्याण’ से ही पिट सकता है। इसमें बहस का सपना देखकर क्रान्ति का प्रॉविडेण्ट फण्ड उठाते हुए छूमन्तर हो जानेवाले शातिर हैं। कल्याण की कारीगरी वाले सपने पर जाए बगैर इस साजिश को समझना मुश्किल होता है। इसलिए आदर्शों के बिना गोलमाल की भी कोई औकात नहीं रह जाती।
मुझे एक झूठी, उबाऊ बहस से सुन्दर लगेगी एक छोटे शब्द की गर्माहट। पर यह गर्माहट है क्या, इसके लिए भी कोई आधार चाहिए। उस आधार की तलाश हो सके तो यूटोपिया मेरे लिए एक आश्वस्त करनेवाला बिन्दु है।
इस बिन्दु से मैं एक रेखा बनाना चाहूँगा।
रेखा को आप जानते ही हैं-वह मुजफ्फर अली की ‘उमराव जान’ और श्याम बेनेगल की ‘जुबैदा’ से भी मिलने जाती रहती है।
शायद यह मेरे सपने का अगम्भीर निष्कर्ष है, लेकिन आदर्श समाजों की कल्पना के लिए गम्भीरता आजकल खतरनाक चीज है। गम्भीर होकर भी यदि मैं कुछ खतरे उठा सकूँ-तो यह मेरे लिए प्रिय सपना होगा। इसलिए कल्पना की दुनिया का कोई भी पक्का ब्ल्यू प्रिण्ट मैं आपको नहीं दे सकता।
आप उसकी तलाश का मजा क्यों किरकिरा करना चाहते हैं ?
चलिए, हैसियत के हिसाब से चालू मुहावरों में, कुछ तलाश करें।
रमेश उपाध्याय सम्पादित ‘कथन’ में यह यूटोपिया कथन दिया था। यही यहाँ का ‘कथन’ बन गया।
असली ‘अब तक छप्पन’ का एनकाउण्टर हीरो दया नायक कचहरियों के चक्कर काट रहा है।
अभी छप्पन हैं, छप्पन सौ साठ भुगतने बाकी हैं।
दुआ करें यह छप्पनिया अकाल न हो !
मुझे हर मजाक में कोई प्यारी चीज नजर आती थी। जैसे भटकटैया के फूल खिले हों तो भी मैं मोगरे वगरैह की सोच सकता था। मोगरी से कपड़े कूटने की ध्वनि में मुझे, धोबियों की छुट्टी कौन से दिन होगी-यह विचार परेशान करता था। उम्र का दोष था। सपने देखते थे और पागल होने की प्रतिष्ठा समझते थे। विवेक और न्याय के सहारे भाषण बेहतर बन जाते थे और पुरस्कार देनेवाले वे सर्वगुण सम्पन्न सेठजी निकलते जो एक सरकारी मान्यता प्राप्त और दूसरी गैर-मान्यता प्राप्त सेठानी रखे हुए लोगों को पूरे मन से उपदेश देते थे। इस तरह यूटोपिया की टोपियाँ उछलती रहती थीं।
डर बढ़े, चेतावनियाँ बढ़ीं, पर सपने देखना नहीं छूटा।
मैं अभी भी मैटिनी शो तक के सपने बदस्तूर देखता हूँ। मैंने पहला उपन्यास लिखा था तो उसकी भूमिका में कहा-
कहते हैं सपनों में कोई क्रम नहीं होता। पात्र भी कभी बबूल होते हुए आम हो जाते हैं, कभी आम होते हुए बबूल। कभी खंडहर, साँप, चोर, उड़ान आपस में जा मिलते हैं। कुछ लोग सपने में रोते हैं, दाँत किटकिटाते हैं, घबरा जाते हैं, चीख पड़ते हैं, उठ जाते हैं, मुस्कुराते हैं या सुबह होने पर लगभग उसे भूल भी जाते हैं। पर, कुछ-बुरे कुछे-अच्छे स्वप्न जब भी आते हैं-याद रह जाते हैं। इनकी अर्थहीनता में भी एक अर्थ होता है और भंग-अंग के बावजूद एक क्रम। अवचेतन तक पहुँचने का यह जादुई रास्ता, ‘स्वप्नविचार’ की पारम्परिक पुस्तिकाओं की व्याख्याओं से ऊपर जाकर एक यात्रा पर ले जाता है। कुछ इससे गुत्थियाँ भी खोल लेते हैं, कुछ इसके दोष से घबराकर हकीमों के पास चले जाते हैं। बावजूद इसके हर आदमी को सपने बगैर कहे आते हैं, और एक यात्रा पर ले जाते हैं। कभी दो किलोमीटर तो कभी दो लाख किलोमीटर भी। हम इन्हें आपस में मिलाये बगैर इनमें सामंजस्य ढूँढ़ने और सुख तथा दुःख की अण्टी मारे बिना रह भी नहीं सकते।
सपनों के साथ यह दिक्कत है कि हम तय करके उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन उतनी ही सुविधा यह है कि उन्हें देखने पर चाहें तो अपने-अपने अर्थ जरूर निकाल सकते हैं।
कहते हैं, जब एक सपने में साँप ने मुँह में पूँछले ली तो उससे कैकुले को कार्बनिक रसायन की बेंजीन रिंग का सूत्र मिल गया था। यानी सपने का अर्थ किसी को जम जाए तो कार्बनिक रसायन का सूत्रपात भी हो जाता है लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि हर सूत्र सपने से उपजता है।
मैं बुरी तरह सपने देखता हूँ। चूँकि सपने देखना न देखना अपने बस में नहीं होता, मैंने भी इन्हें देखा। आप सबकी तरह मैंने भी कभी नहीं चाहा कि स्वप्न, फ्रायड या युंग जैसों की सैद्धान्तिकता से आक्रान्त होकर आएँ या प्रसव पीड़ा की नीम बेहोशी में अखिल विश्व के पाप निवारक ईश्वर के अवतार की सुखद आकाशवाणी के प्ले-बैक के साथ।
सपनों की प्रकृति के अनुरूप भयंकर रूप से एक-दूसरे में गुमे हुए काल, स्थान और पात्रों के साथ मैंने अपने सपनों की यथासम्भव जमावट का एक चालू चिट्ठा पेश किया और ऊपर से कहा-‘यदि तावदयं स्वप्नों धन्यमप्रतिबोधनम्।’ जैसा कि भास की ‘स्वप्नवासवदत्ता’ में आता है-यदि यह स्वप्न है, तो न जागना ही अच्छा होता।
मेरा सपना, इस लिहाज से छुपा हुआ नहीं है। आदर्श मुझे खींचता है, बनाता है, पैमाना रखता है, एक तलाश के लिए प्रवृत्त करता है। हर आदमी को रोटी, कपड़ा मकान दिये जाने का स्टीरियोटाइप क्रान्तिवादी सपना आजकल कवि के उस गेटअप की तरह है जिसे फटे कुर्ते, बढ़े बाल और झोले के सहारे स्थायी मान लिया गया है। मैं अपने सपने में इस चालूपन का प्रतिकार करता हूँ, कभी-कभी इसीलिए बहुत बुरे सपने भी आते हैं।
मैं स्वनामधन्य कलावादी की तरह चाँद पर बैठकर धरती को देखता हूँ तो एक मनुष्य की स्थिति समूची पृथ्वी के मुकाबले चींटी से भी गयी-बीती नजर आती है। पर, यह देखने के लिए चाँद पर जाना जरूरी है। यह भी तभी होगा जब वही मनुष्य चाँद पर जाने लायक वैज्ञानिक इन्तजाम करे। इसलिए आदर्श समाज और नैतिक आस्थाएँ मुझे शक्ति देती हैं। करुणा और प्रेम सपने की ईंट-सीमेण्ट बन जाते हैं। पर, सच्चे जीवन के लिए वैज्ञानिक तर्कवाद चाहिए।
हर व्यक्तिगत स्वप्न, दूसरे के स्वप्न में हस्तक्षेप के साथ बनता है। जैसे पाँच सितारा होटल में शानदार दावत का स्वप्न, वेटर के उस स्वप्न पर चढ़ा मिलेगा जिसमें वह वेटर दावत से मिली टिप के पैसे गिनते हुए अपने पिता की दवाई का ध्यान करेगा। लेकिन, शायद आदर्श समाज सपनों में हस्तक्षेप की बजाय सपनों में साझे से शक्ति लेता होगा। इसलिए ‘कौन बनेगा करोड़पति का स्वप्निल झाँसा, ‘कौन करेगा करोड़ों का कल्याण’ से ही पिट सकता है। इसमें बहस का सपना देखकर क्रान्ति का प्रॉविडेण्ट फण्ड उठाते हुए छूमन्तर हो जानेवाले शातिर हैं। कल्याण की कारीगरी वाले सपने पर जाए बगैर इस साजिश को समझना मुश्किल होता है। इसलिए आदर्शों के बिना गोलमाल की भी कोई औकात नहीं रह जाती।
मुझे एक झूठी, उबाऊ बहस से सुन्दर लगेगी एक छोटे शब्द की गर्माहट। पर यह गर्माहट है क्या, इसके लिए भी कोई आधार चाहिए। उस आधार की तलाश हो सके तो यूटोपिया मेरे लिए एक आश्वस्त करनेवाला बिन्दु है।
इस बिन्दु से मैं एक रेखा बनाना चाहूँगा।
रेखा को आप जानते ही हैं-वह मुजफ्फर अली की ‘उमराव जान’ और श्याम बेनेगल की ‘जुबैदा’ से भी मिलने जाती रहती है।
शायद यह मेरे सपने का अगम्भीर निष्कर्ष है, लेकिन आदर्श समाजों की कल्पना के लिए गम्भीरता आजकल खतरनाक चीज है। गम्भीर होकर भी यदि मैं कुछ खतरे उठा सकूँ-तो यह मेरे लिए प्रिय सपना होगा। इसलिए कल्पना की दुनिया का कोई भी पक्का ब्ल्यू प्रिण्ट मैं आपको नहीं दे सकता।
आप उसकी तलाश का मजा क्यों किरकिरा करना चाहते हैं ?
चलिए, हैसियत के हिसाब से चालू मुहावरों में, कुछ तलाश करें।
रमेश उपाध्याय सम्पादित ‘कथन’ में यह यूटोपिया कथन दिया था। यही यहाँ का ‘कथन’ बन गया।
असली ‘अब तक छप्पन’ का एनकाउण्टर हीरो दया नायक कचहरियों के चक्कर काट रहा है।
अभी छप्पन हैं, छप्पन सौ साठ भुगतने बाकी हैं।
दुआ करें यह छप्पनिया अकाल न हो !
यशवन्त व्यास
1
जड़ हे ! जड़ हे !! जड़ हे !!!
पहले तो डीबीडीएन ने कनॉट प्लेस के कुत्ते देखे, फिर आगे चलकर बोर्ड देखा,
बोर्ड पर ‘राजीव चौक’ लिखा था।
उनका मन खिल गया। नीचे गिरकर फट गये जामुन से ज्यों रस छलकर फुटपाथ को बैंगनी मिठास देता है, डीबीडीएन को कनॉट प्लेस के राजीव चौक में तब्दील होने की मिठास मिली।
प्रचार था कि उनका नाम दलित बन्धु दुखभंजन नाथ नहीं है। जब वे बच्चे थे तब मालगाड़ी के डिब्बों से कोयला चुराते थे। बाबू ने एक बार पकड़ लिया। पीठ पर डुक्का पड़ा। तब इन्होंने बाबू के संकेत में कहा-डब्बा डुक्का नॉट ! यानी डिब्बे के पीछे चलो बाबू, डुक्का न दो। बाबू समझ गया और चोरी के प्रथमांश को अर्पित करने का बीज पहली बार वहीं पड़ा। इलाके में काम करना हो तो ‘डब्बा बब्बा डुक्का नॉट’ से बड़ा कोई मन्तर नहीं बना। उनका नाम डीबीडीएन इसी मन्तर पर पड़ा। कहते तो यह भी हैं कि उनके पिताजी ने दीनबन्धु दीनानाथ के नाम पर उन्हें नाम दिया था पर जब दलित आन्दोलन ने जोर पकड़ा और उधर एक फिल्म आयी जिसमें खलनायक सदाशिव अमरापुरकर का नाम डीबीडीएन पाया गया तो वे तेजी से भाग्य का लेखा समझ गये। यों कथाकार-कवि समाजकर्मी डीबीडीएन का पूरा नाम हुआ-दलित बन्धु दुखभंजन नाथ। अलबत्ता माल गाड़ी के डिब्बे और डुक्के उन्हें अभी भी उतने ही सताते हैं। आजकल वे कवि हैं।
तो, ऐसा हमारा कवि डीबीडीएन आगे बढ़ा।
रीगल के पोस्टर से टाँगें बाहर आ रही थीं। पीछे के तीन मंजिले कॉफी हाउस में न जाकर कवि हनुमान मन्दिर गया। कुछ भक्तिनों को देखा। मनन किया। पैंतालीस डिग्री पर आँखें उठायीं और एक गहरी साँस ली-लिखने को क्या बचा रह गया है। तभी एक कुत्ता काँय-काँय करता भाग खड़ा हुआ।
कवि की आत्मा दरियागंज हो गयी, मन प्राग हो गया, दिमाग आयोवा और आँखें टेम्स !
सड़क दिल्ली की, संकट कवि का। दिल्ली के ठंगों में ठगा-सा खड़ा कवि। लगे कि जैसे कवि की कटी जेब से गिरी स्त्री, बचा विमर्श। वह अर्श, यह फर्श !
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सीवर लाइन में इस बीच कितना मैला बह गया है ! दुनिया बदल गयी। कवि अपनी उम्र और कविताओं का आँकड़ा मिलाकर देखने लगा। उसे अचानक अहसास हुआ कि पिछले अनेक सालों में उसने 160 अध्यक्षताएँ कीं, 1001 संस्मरण सुनाये, 1500 बहसें कीं, लगभग 90 बार श्लील-अश्लील हुआ, कम-से-कम 10 बार गाली-गलौज का स्तर उठाकर राष्ट्रीय किया। अरे दलित बन्धु दुखभंजन नाथ, फिर भी ग्रासरूट लेवल पर फर्क न पड़ा। ओह डब्बा बब्बा डुक्का नॉट-तू करोड़पति भी न बना। कुलपति भी नहीं बना। कुलशील के स्तर पर रैडिकल होते हुए भी नामाकूल डीबीडीएन, तू असली दुनिया की क्रान्ति में कुछ न कर सका, तुझसे देश के अन्तिम आदमी को क्या मिला ?
हाय भारत देश ! हाय इण्डिया गेट ! अरे मिनाजुद्दीन पुलकी हवाओ ! ओय दारूकुट्टे सम्पादकों, ओय-होय शातिर मीडिया सेवकों ! ओह धौला कुआँ के ट्रैफिक पुलिस वालो ! सुनो क्लब के धरनार्थियों ! इण्डिया इण्टरनेशनल सेण्टर की सड़क की चिरकनाइयो ! सुनो-यह कवि अब नहीं रुकेगा। वह जड़ों की ओर लौट रहा है।
कवि को बोधप्राप्ति हो गयी।
वह बीकानेर हाउस से डीलक्स बस में बैठकर जड़ों की ओर लौट गया।
कवि की जड़ें पूरी धरती पर होती हैं। मगर वह जब उनकी तरफ लौटना चाहे तो चयन के विकल्पों का प्रावधान है।
उसकी जड़ें नायला में थीं। वही जयपुर के पास वाला नायला। मतलब वही-अहा ग्राम्य जीवन भी क्या है, हैण्डपम्प में पानी नहीं आता, सड़क सन् साठ की फिल्मों की प्रेरणा लेकर सौन्दर्य टिकाए चली आ रही है। कई लोकल अखबारों के स्ट्रिंगरों के लिए महीने का मामूली बिल बनाने में मदद करने का पूरा इन्तजाम। सड़क, स्कूल वगैरह पर कई सालों से लिख रहे हैं, आगे भी लिखते रहेंगे। ईश्वर ने अगर चाहा तो अखबारवालों की अगली पीढ़ियाँ भी इन्हीं समाचारों से कमा खाएँगी।
पर, डीबीडीएन के लिए नायला महज नायला नहीं था। वह कवि की वैश्विक दृष्टि में ग्लोबलाइजेशन की पहली प्रयोगशाला थी। यह वही गाँव था जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को दिखाने के लिए चुना गया था।
कवि ने क्लिंटन के फर्टिलाइजर से सींची जा रही जडों की ओर हसरत भरी निगाहों से देखा। वह भी मोनिका और हिलेरी की कथाओं का निष्ठावान वाचक था। वह भी केसरिया बालम होना जानता था। वह जड़ों के हरेपन में विश्व कुटुम्ब का प्रवाह देखना चाहता था। वह लगना चाहता था-सामन्ती इतिहास के प्रदेश में जन-जड़ों को देखता कवि ! वह जड़ों का सुख उठाना चाहता था। वह लड़कियों से पिटने पर व्यभिचार का शास्त्र लिख सकता था। पिता पकड़ में आ जाए तो उसे कहानी बनाकर बेच सकता था। शौचालय में बनायी पैंसिल की आकृतियों को कला के नमूनों में बदलकर श्लील-अश्लील की बहस खड़ी करवा सकता था। उसे कुछ करना ही था। उसे जड़ें चाहिए थीं।
क्या आपको पता है कि कोई भी अपनी जड़ों को कैसे देख सकता है ? अपनी जड़ें होती क्या हैं ? क्या आदमी की जड़ पेड़ की जड़ की तरह ही होती है ? अधिकांश कवियों की जड़ गाँव में ही क्यों होती है ? कवि की जड़ शेष मनुष्यों की जड़ से भिन्न होती है ? तो, डीबीडीएन की जड़ें और किसी अन्य रचनाकार की जड़ें भी कुछ भिन्न होती होंगी, ‘डब्बा बब्बा डुक्का नॉट’ की जड़ें कुछ खास होती होंगी। क्या गारण्टी है कि कवि जड़ों की ओर लौटेगा तो अपनी ही जड़ों पर पहुँचेगा, किसी और की जड़ को अपनी जड़ समझकर उसी पर लटूम नहीं जाएगा ? जड़ों पर कोई बिल्ला, बैनर पट्टी या निशान तो होता होगा।
यह संशय में डालने वाला मसला है। कवि एक पल ठिठकता है, फिर खिल जाता है।
कवि संशय को शक्ति में बदलना जानता है। चिन्ता न करें, वह जड़ों पर आठ लम्बी कविताएँ लिख चुका है। कविताएँ उसकी कुदाल हैं। मिट्टी खोदकर जड़ों तक पहुँचने का इन्तजाम है उसके पास। ज्यादा जरूरत पड़ी तो दो-तीन कविताएँ और लिख देगा। कुदालों की संख्या बढ़ जाएगी।
जड़ों की ओर लौटने के लिए वह नायला की जमीन को छूकर देखने लगा। बदरपुर से थोड़ी अलग है। यमुना पुश्ते से भी थोड़ी अलग है। ओह, इन्दौर के रेसकोर्स रोड और मुम्बई की चौपाटी से भी अलग है। जब सबसे अलग है तो अद्वितीय है। अद्वितीयता तो डीबीडीएन की ही खासियत है। चलो, शान्ति हुई। एक लक्षण पकड़ में आया, अब वह निबट लेगा।
कवि अपनी अद्वितीयता पर सोचने लगा। मौं सम कौन कुटिल, खल, कामी ?
वह दलित है क्योंकि उसने प्रमाण पत्र बनवा रखा है। वह ब्राह्मण है क्योंकि उसके नाम में वह गन्ध आती है। वह ठाकुर है क्योंकि उसने कई वध किये हैं। वह स्त्रियों का उन्नायक है क्योंकि सर्वाधिक अश्लील कथाएँ रचने का उस पर आरोप है। वह अकेला है, अपनी तरह का अकेला। आह वह चण्डूखाने से लेकर अंसारी रोड तक एक-सा सनसनाता तीर ! वह कुक्कड़ की टाँगों से लेकर नुक्कड़ के लोकार्पण के फीतों तक पवित्रतम निमित्त।
चित्त और वित्त की यह अद्वितीयता उसे मीठी बेहोशी देने लगी।
वह नीचे बैठ गया।
जहाँ बैठा था, वे पंचायत भवननुमा जगह पर बनी सीढ़ियाँ थीं। मीठी बेहोशी में उसने खेत-खलिहान सिटी बसें, गिद्ध कौए, कलाली, किताबें वगैरह देखीं। भागते-चलते बच्चे देखे। नाचता हुआ क्लिंटन देखा। उस पर फूल गिरे थे। घूँघट में गाँव की औरतें उसके आसपास घूमर ले रही थीं। नायला जगर-मगर कर रहा था। उसी जगर-मगर में क्लिंटन ने एक कम्प्यूटर दिया।
शॉट फ्रीज हो गया।
डीबीडीएन की तन्द्रा टूट गयी। सामने एक बकरी मुँह चला रही थी। पीछे चार भले लोग बकरी पर टूट पड़ने के अन्दाज में ! बकरी ने संवेदनाशीलता के आगार को पहचान लिया। कवि के पीछे शरण ली।
कवि और भले लोगों के बीच संवाद आरम्भ हुआ।
‘‘आप कौन हैं ?’’
‘‘मैं जड़ों की तलाश में आया हूँ।’’
‘‘किसकी जड़ें चाहिए-शकरकन्द की, मूली की या बरगद की ?’’
‘‘अपनी जड़ें।’’
‘‘तो जाओ, खेत में उग जाओ ।’’
कवि उनकी हालत पर हँसा। पंचायत में देश की जड़ें होती हैं, पंचायत की सीढ़ियों पर बैठा कवि अपनी जड़ों की ओर लौटकर देश को आगे बढ़ाना चाहता था। ऐसे गम्भीर काम को वे कमअक्ल कैसे समझ सकते थे, जो एक बकरी के पीछे पड़े थे !
बकरी ने कवि को देखा। कवि ने बकरी को ऐसे, जैसे आश्वासन दिया हो कि अगली बार तुझ पर पाँच कविताएँ लिखूँगा। अभी जरा जड़ मूर्खों से निबट लूँ, अपनी जड़ें तलाश लूँ।
‘‘तुम्हें जड़ों के बारे में कुछ नहीं पता। जड़ों की ओर लौटना बड़ा गम्भीर काम है। बीस साल रेडियो, टीवी अखबार, पत्रिका और व्याख्यान के लम्बे व्यायाम के बाद मुझे समझ में आया कि जड़ों की ओर लौटना चाहिए। तुम इस पचड़े में मत पड़ों। तुम तो इतना भर बताओ कि बकरी के पीछे क्यों पड़े हो ?’’ कवि ने बिल्कुल इस तरह चेहरा बनाया जैसे प्रसार भारती का फोकट अनुबन्ध पकड़ा रहा हो या कमीशण्ड कार्यक्रम का सार किसी घुटे हुए सम्पादक से शेयर कर रहा हो।
जाहिर है, वे चारों न घुटे हुए सम्पादक थे, न प्रोग्राम पास करनेवाले अफसर ! वे गाँव के लोग थे। उनका लक्ष्य बकरी थी। वे जड़-बहस में नहीं पड़ना चाहते थे।
‘‘पंचायत छोड़ो। थोड़ा सा हट जाओ। ये बकरी उस कम्प्यूटर का प्लग चबा गयी है जो बिल क्लिटन साहब के यहाँ आने के मौके पर हमें मिला था। हम इसे ठीक करना चाहते हैं।’’
बकरी मिमियाई।
कवि गरज उठा, ‘‘इसने कम्प्यूटर का प्लग चबाया है। जब कमप्यूटर खुला पड़ा था, तब तुम क्या कर रहे थे ?’’
‘‘जब से कम्प्यूटर आया, तब से खुला पड़ा था। वह एक जादुई डिब्बा था जो धूल खाता, हमें डराता था। बिजली नहीं थी। हमारे पास अलग से कोई मेज नहीं थी, फिर भी हमने कम्प्यूटर के लिए जगह निकाली। हम शपथपूर्वक कहना चाहते हैं कि हैण्डपम्प सूखा पड़ा है, वह देखते-देखते हमने बकरी को जरा सा हड़काया था। यह उछल भागी और कम्प्यूटर तक जा पहुँची। वहीं उसने प्लग चबा लिया। हम इसके पेट से वह प्लग निकालकर कम्प्यूटर में वापस लगाना चाहते हैं वरना क्लिंटन साहब के प्रति यह गुनाह हो जाएगा। हम क्रान्ति और कम्प्यूटर तक जाते-जाते चोरी गुमशुदागी के आरोप में मारे जाएँगे।’’
कवि की गरज शान्त हो गयी। उन्होंने छँटे हुए सॉफ्टवेयर-हार्डवेयर ज्ञाता की तरह बकरी की गरदन पर हाथ धरा। उसकी आँखों में आँखें डालीं। क्लिंटन की भाँति मुस्कुराये, तार से तार मिल गये। बकरी की आँखें स्क्रीन में बदल गयीं। सारा डेटा खुल पड़ा था। पहली फाइल में जड़ें ही जड़ें थीं, वह जड़ें जिनकी तरफ लौटने के लिए कवि बेताब होकर दिल्ली छोड़ आया था।
बकरी के कान माउस हो गये। पीठ की-बोर्ड में बदल गयी, मुँह से प्रिण्ट निकलने लगे।
यह जादुई यथार्थवाद था और इसमें मौलिकता का स्तर इतना ऊँचा था कि किसी आचार्य से मदद लेने की जरूरत नहीं थी। स्थापनाएँ साफ थीं। मोनिका का वालपेपर स्क्रीन को मोहक बना रहा था। बीच की झपकी में एक स्क्रीन सेवर चला तो वह जड़ों की सूक्ष्म रचना से बना निकला। गाँव की को-ऑपरेटिव दूध सोसायटी, महिला उत्थान समिति, गिट्टी-सड़क गड्ढे आदि से विहीन रेशमी सड़क और क्लिंटन की टी-शर्ट भी खुली। एक फाइल में ‘प्रेजेण्टेशन’ बना निकला, जो बताता था कि नायला विश्व का पहला कम्प्यूटर ग्राम बनकर अपनी जड़ों से कैसे आकाश छूने जा रहा है। प्रेजेण्टेशन में हर बार एक ग्राफिक आता था। जिसमें पर्यटन मन्त्री घूमर लेता दिखता था। संगीत भी था, केसरिया बालम पधारो नी म्हारे देस ! नायला एकदम ग्लोबल ग्राम बन जाता था और देहाती, क्लिंटन का टी शर्ट पहनकर हैण्डपम्प से टैंकर के टैंकर पानी भरते थे।
बकरी की पीठ पर उँगलियाँ चल रही थीं, नयी-नयी चीजें खुल रही थीं। मुँह से प्रिण्ट पर प्रिण्ट गिर रहे थे। कवि कम्प्यूटर को इण्टरनेट से जोड़कर साइबर स्पेस में जाना चाहता था कि कनेक्शन कट गया।
कवि की लय टूट गयी। जड़ों से चल रहा रास छूट गया।
सारा उपक्रम थम गया।
सामने वही देहाती खड़े थे। बकरी उछलकर सूखे हैण्डपम्प की ओर दौड़ पड़ी थी।
कवि अब रुक नहीं सकता था। डीबीडीएन को कर्तव्य पुकार रहा था। जड़ों के पास जाकर वह उन्हें खोना नहीं चाहता था। तो भागा कवि आगे-आगे। देहाती उसके पीछे। नीचे धूल मिट्टी गड्ढे ऊपर तीखी धूप।
देहाती चिल्ला रहे थे-बकरी चोर। पकड़ों। कवि कह रहा था-आ लौट आ जड़ों की ओर आ, चल तुझे साइबर स्पेस ले चलूँ।
चोर, जड़ें और साइबर स्पेस !
समाँ बँध गया, माहौल बन गया !!
उनका मन खिल गया। नीचे गिरकर फट गये जामुन से ज्यों रस छलकर फुटपाथ को बैंगनी मिठास देता है, डीबीडीएन को कनॉट प्लेस के राजीव चौक में तब्दील होने की मिठास मिली।
प्रचार था कि उनका नाम दलित बन्धु दुखभंजन नाथ नहीं है। जब वे बच्चे थे तब मालगाड़ी के डिब्बों से कोयला चुराते थे। बाबू ने एक बार पकड़ लिया। पीठ पर डुक्का पड़ा। तब इन्होंने बाबू के संकेत में कहा-डब्बा डुक्का नॉट ! यानी डिब्बे के पीछे चलो बाबू, डुक्का न दो। बाबू समझ गया और चोरी के प्रथमांश को अर्पित करने का बीज पहली बार वहीं पड़ा। इलाके में काम करना हो तो ‘डब्बा बब्बा डुक्का नॉट’ से बड़ा कोई मन्तर नहीं बना। उनका नाम डीबीडीएन इसी मन्तर पर पड़ा। कहते तो यह भी हैं कि उनके पिताजी ने दीनबन्धु दीनानाथ के नाम पर उन्हें नाम दिया था पर जब दलित आन्दोलन ने जोर पकड़ा और उधर एक फिल्म आयी जिसमें खलनायक सदाशिव अमरापुरकर का नाम डीबीडीएन पाया गया तो वे तेजी से भाग्य का लेखा समझ गये। यों कथाकार-कवि समाजकर्मी डीबीडीएन का पूरा नाम हुआ-दलित बन्धु दुखभंजन नाथ। अलबत्ता माल गाड़ी के डिब्बे और डुक्के उन्हें अभी भी उतने ही सताते हैं। आजकल वे कवि हैं।
तो, ऐसा हमारा कवि डीबीडीएन आगे बढ़ा।
रीगल के पोस्टर से टाँगें बाहर आ रही थीं। पीछे के तीन मंजिले कॉफी हाउस में न जाकर कवि हनुमान मन्दिर गया। कुछ भक्तिनों को देखा। मनन किया। पैंतालीस डिग्री पर आँखें उठायीं और एक गहरी साँस ली-लिखने को क्या बचा रह गया है। तभी एक कुत्ता काँय-काँय करता भाग खड़ा हुआ।
कवि की आत्मा दरियागंज हो गयी, मन प्राग हो गया, दिमाग आयोवा और आँखें टेम्स !
सड़क दिल्ली की, संकट कवि का। दिल्ली के ठंगों में ठगा-सा खड़ा कवि। लगे कि जैसे कवि की कटी जेब से गिरी स्त्री, बचा विमर्श। वह अर्श, यह फर्श !
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सीवर लाइन में इस बीच कितना मैला बह गया है ! दुनिया बदल गयी। कवि अपनी उम्र और कविताओं का आँकड़ा मिलाकर देखने लगा। उसे अचानक अहसास हुआ कि पिछले अनेक सालों में उसने 160 अध्यक्षताएँ कीं, 1001 संस्मरण सुनाये, 1500 बहसें कीं, लगभग 90 बार श्लील-अश्लील हुआ, कम-से-कम 10 बार गाली-गलौज का स्तर उठाकर राष्ट्रीय किया। अरे दलित बन्धु दुखभंजन नाथ, फिर भी ग्रासरूट लेवल पर फर्क न पड़ा। ओह डब्बा बब्बा डुक्का नॉट-तू करोड़पति भी न बना। कुलपति भी नहीं बना। कुलशील के स्तर पर रैडिकल होते हुए भी नामाकूल डीबीडीएन, तू असली दुनिया की क्रान्ति में कुछ न कर सका, तुझसे देश के अन्तिम आदमी को क्या मिला ?
हाय भारत देश ! हाय इण्डिया गेट ! अरे मिनाजुद्दीन पुलकी हवाओ ! ओय दारूकुट्टे सम्पादकों, ओय-होय शातिर मीडिया सेवकों ! ओह धौला कुआँ के ट्रैफिक पुलिस वालो ! सुनो क्लब के धरनार्थियों ! इण्डिया इण्टरनेशनल सेण्टर की सड़क की चिरकनाइयो ! सुनो-यह कवि अब नहीं रुकेगा। वह जड़ों की ओर लौट रहा है।
कवि को बोधप्राप्ति हो गयी।
वह बीकानेर हाउस से डीलक्स बस में बैठकर जड़ों की ओर लौट गया।
कवि की जड़ें पूरी धरती पर होती हैं। मगर वह जब उनकी तरफ लौटना चाहे तो चयन के विकल्पों का प्रावधान है।
उसकी जड़ें नायला में थीं। वही जयपुर के पास वाला नायला। मतलब वही-अहा ग्राम्य जीवन भी क्या है, हैण्डपम्प में पानी नहीं आता, सड़क सन् साठ की फिल्मों की प्रेरणा लेकर सौन्दर्य टिकाए चली आ रही है। कई लोकल अखबारों के स्ट्रिंगरों के लिए महीने का मामूली बिल बनाने में मदद करने का पूरा इन्तजाम। सड़क, स्कूल वगैरह पर कई सालों से लिख रहे हैं, आगे भी लिखते रहेंगे। ईश्वर ने अगर चाहा तो अखबारवालों की अगली पीढ़ियाँ भी इन्हीं समाचारों से कमा खाएँगी।
पर, डीबीडीएन के लिए नायला महज नायला नहीं था। वह कवि की वैश्विक दृष्टि में ग्लोबलाइजेशन की पहली प्रयोगशाला थी। यह वही गाँव था जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को दिखाने के लिए चुना गया था।
कवि ने क्लिंटन के फर्टिलाइजर से सींची जा रही जडों की ओर हसरत भरी निगाहों से देखा। वह भी मोनिका और हिलेरी की कथाओं का निष्ठावान वाचक था। वह भी केसरिया बालम होना जानता था। वह जड़ों के हरेपन में विश्व कुटुम्ब का प्रवाह देखना चाहता था। वह लगना चाहता था-सामन्ती इतिहास के प्रदेश में जन-जड़ों को देखता कवि ! वह जड़ों का सुख उठाना चाहता था। वह लड़कियों से पिटने पर व्यभिचार का शास्त्र लिख सकता था। पिता पकड़ में आ जाए तो उसे कहानी बनाकर बेच सकता था। शौचालय में बनायी पैंसिल की आकृतियों को कला के नमूनों में बदलकर श्लील-अश्लील की बहस खड़ी करवा सकता था। उसे कुछ करना ही था। उसे जड़ें चाहिए थीं।
क्या आपको पता है कि कोई भी अपनी जड़ों को कैसे देख सकता है ? अपनी जड़ें होती क्या हैं ? क्या आदमी की जड़ पेड़ की जड़ की तरह ही होती है ? अधिकांश कवियों की जड़ गाँव में ही क्यों होती है ? कवि की जड़ शेष मनुष्यों की जड़ से भिन्न होती है ? तो, डीबीडीएन की जड़ें और किसी अन्य रचनाकार की जड़ें भी कुछ भिन्न होती होंगी, ‘डब्बा बब्बा डुक्का नॉट’ की जड़ें कुछ खास होती होंगी। क्या गारण्टी है कि कवि जड़ों की ओर लौटेगा तो अपनी ही जड़ों पर पहुँचेगा, किसी और की जड़ को अपनी जड़ समझकर उसी पर लटूम नहीं जाएगा ? जड़ों पर कोई बिल्ला, बैनर पट्टी या निशान तो होता होगा।
यह संशय में डालने वाला मसला है। कवि एक पल ठिठकता है, फिर खिल जाता है।
कवि संशय को शक्ति में बदलना जानता है। चिन्ता न करें, वह जड़ों पर आठ लम्बी कविताएँ लिख चुका है। कविताएँ उसकी कुदाल हैं। मिट्टी खोदकर जड़ों तक पहुँचने का इन्तजाम है उसके पास। ज्यादा जरूरत पड़ी तो दो-तीन कविताएँ और लिख देगा। कुदालों की संख्या बढ़ जाएगी।
जड़ों की ओर लौटने के लिए वह नायला की जमीन को छूकर देखने लगा। बदरपुर से थोड़ी अलग है। यमुना पुश्ते से भी थोड़ी अलग है। ओह, इन्दौर के रेसकोर्स रोड और मुम्बई की चौपाटी से भी अलग है। जब सबसे अलग है तो अद्वितीय है। अद्वितीयता तो डीबीडीएन की ही खासियत है। चलो, शान्ति हुई। एक लक्षण पकड़ में आया, अब वह निबट लेगा।
कवि अपनी अद्वितीयता पर सोचने लगा। मौं सम कौन कुटिल, खल, कामी ?
वह दलित है क्योंकि उसने प्रमाण पत्र बनवा रखा है। वह ब्राह्मण है क्योंकि उसके नाम में वह गन्ध आती है। वह ठाकुर है क्योंकि उसने कई वध किये हैं। वह स्त्रियों का उन्नायक है क्योंकि सर्वाधिक अश्लील कथाएँ रचने का उस पर आरोप है। वह अकेला है, अपनी तरह का अकेला। आह वह चण्डूखाने से लेकर अंसारी रोड तक एक-सा सनसनाता तीर ! वह कुक्कड़ की टाँगों से लेकर नुक्कड़ के लोकार्पण के फीतों तक पवित्रतम निमित्त।
चित्त और वित्त की यह अद्वितीयता उसे मीठी बेहोशी देने लगी।
वह नीचे बैठ गया।
जहाँ बैठा था, वे पंचायत भवननुमा जगह पर बनी सीढ़ियाँ थीं। मीठी बेहोशी में उसने खेत-खलिहान सिटी बसें, गिद्ध कौए, कलाली, किताबें वगैरह देखीं। भागते-चलते बच्चे देखे। नाचता हुआ क्लिंटन देखा। उस पर फूल गिरे थे। घूँघट में गाँव की औरतें उसके आसपास घूमर ले रही थीं। नायला जगर-मगर कर रहा था। उसी जगर-मगर में क्लिंटन ने एक कम्प्यूटर दिया।
शॉट फ्रीज हो गया।
डीबीडीएन की तन्द्रा टूट गयी। सामने एक बकरी मुँह चला रही थी। पीछे चार भले लोग बकरी पर टूट पड़ने के अन्दाज में ! बकरी ने संवेदनाशीलता के आगार को पहचान लिया। कवि के पीछे शरण ली।
कवि और भले लोगों के बीच संवाद आरम्भ हुआ।
‘‘आप कौन हैं ?’’
‘‘मैं जड़ों की तलाश में आया हूँ।’’
‘‘किसकी जड़ें चाहिए-शकरकन्द की, मूली की या बरगद की ?’’
‘‘अपनी जड़ें।’’
‘‘तो जाओ, खेत में उग जाओ ।’’
कवि उनकी हालत पर हँसा। पंचायत में देश की जड़ें होती हैं, पंचायत की सीढ़ियों पर बैठा कवि अपनी जड़ों की ओर लौटकर देश को आगे बढ़ाना चाहता था। ऐसे गम्भीर काम को वे कमअक्ल कैसे समझ सकते थे, जो एक बकरी के पीछे पड़े थे !
बकरी ने कवि को देखा। कवि ने बकरी को ऐसे, जैसे आश्वासन दिया हो कि अगली बार तुझ पर पाँच कविताएँ लिखूँगा। अभी जरा जड़ मूर्खों से निबट लूँ, अपनी जड़ें तलाश लूँ।
‘‘तुम्हें जड़ों के बारे में कुछ नहीं पता। जड़ों की ओर लौटना बड़ा गम्भीर काम है। बीस साल रेडियो, टीवी अखबार, पत्रिका और व्याख्यान के लम्बे व्यायाम के बाद मुझे समझ में आया कि जड़ों की ओर लौटना चाहिए। तुम इस पचड़े में मत पड़ों। तुम तो इतना भर बताओ कि बकरी के पीछे क्यों पड़े हो ?’’ कवि ने बिल्कुल इस तरह चेहरा बनाया जैसे प्रसार भारती का फोकट अनुबन्ध पकड़ा रहा हो या कमीशण्ड कार्यक्रम का सार किसी घुटे हुए सम्पादक से शेयर कर रहा हो।
जाहिर है, वे चारों न घुटे हुए सम्पादक थे, न प्रोग्राम पास करनेवाले अफसर ! वे गाँव के लोग थे। उनका लक्ष्य बकरी थी। वे जड़-बहस में नहीं पड़ना चाहते थे।
‘‘पंचायत छोड़ो। थोड़ा सा हट जाओ। ये बकरी उस कम्प्यूटर का प्लग चबा गयी है जो बिल क्लिटन साहब के यहाँ आने के मौके पर हमें मिला था। हम इसे ठीक करना चाहते हैं।’’
बकरी मिमियाई।
कवि गरज उठा, ‘‘इसने कम्प्यूटर का प्लग चबाया है। जब कमप्यूटर खुला पड़ा था, तब तुम क्या कर रहे थे ?’’
‘‘जब से कम्प्यूटर आया, तब से खुला पड़ा था। वह एक जादुई डिब्बा था जो धूल खाता, हमें डराता था। बिजली नहीं थी। हमारे पास अलग से कोई मेज नहीं थी, फिर भी हमने कम्प्यूटर के लिए जगह निकाली। हम शपथपूर्वक कहना चाहते हैं कि हैण्डपम्प सूखा पड़ा है, वह देखते-देखते हमने बकरी को जरा सा हड़काया था। यह उछल भागी और कम्प्यूटर तक जा पहुँची। वहीं उसने प्लग चबा लिया। हम इसके पेट से वह प्लग निकालकर कम्प्यूटर में वापस लगाना चाहते हैं वरना क्लिंटन साहब के प्रति यह गुनाह हो जाएगा। हम क्रान्ति और कम्प्यूटर तक जाते-जाते चोरी गुमशुदागी के आरोप में मारे जाएँगे।’’
कवि की गरज शान्त हो गयी। उन्होंने छँटे हुए सॉफ्टवेयर-हार्डवेयर ज्ञाता की तरह बकरी की गरदन पर हाथ धरा। उसकी आँखों में आँखें डालीं। क्लिंटन की भाँति मुस्कुराये, तार से तार मिल गये। बकरी की आँखें स्क्रीन में बदल गयीं। सारा डेटा खुल पड़ा था। पहली फाइल में जड़ें ही जड़ें थीं, वह जड़ें जिनकी तरफ लौटने के लिए कवि बेताब होकर दिल्ली छोड़ आया था।
बकरी के कान माउस हो गये। पीठ की-बोर्ड में बदल गयी, मुँह से प्रिण्ट निकलने लगे।
यह जादुई यथार्थवाद था और इसमें मौलिकता का स्तर इतना ऊँचा था कि किसी आचार्य से मदद लेने की जरूरत नहीं थी। स्थापनाएँ साफ थीं। मोनिका का वालपेपर स्क्रीन को मोहक बना रहा था। बीच की झपकी में एक स्क्रीन सेवर चला तो वह जड़ों की सूक्ष्म रचना से बना निकला। गाँव की को-ऑपरेटिव दूध सोसायटी, महिला उत्थान समिति, गिट्टी-सड़क गड्ढे आदि से विहीन रेशमी सड़क और क्लिंटन की टी-शर्ट भी खुली। एक फाइल में ‘प्रेजेण्टेशन’ बना निकला, जो बताता था कि नायला विश्व का पहला कम्प्यूटर ग्राम बनकर अपनी जड़ों से कैसे आकाश छूने जा रहा है। प्रेजेण्टेशन में हर बार एक ग्राफिक आता था। जिसमें पर्यटन मन्त्री घूमर लेता दिखता था। संगीत भी था, केसरिया बालम पधारो नी म्हारे देस ! नायला एकदम ग्लोबल ग्राम बन जाता था और देहाती, क्लिंटन का टी शर्ट पहनकर हैण्डपम्प से टैंकर के टैंकर पानी भरते थे।
बकरी की पीठ पर उँगलियाँ चल रही थीं, नयी-नयी चीजें खुल रही थीं। मुँह से प्रिण्ट पर प्रिण्ट गिर रहे थे। कवि कम्प्यूटर को इण्टरनेट से जोड़कर साइबर स्पेस में जाना चाहता था कि कनेक्शन कट गया।
कवि की लय टूट गयी। जड़ों से चल रहा रास छूट गया।
सारा उपक्रम थम गया।
सामने वही देहाती खड़े थे। बकरी उछलकर सूखे हैण्डपम्प की ओर दौड़ पड़ी थी।
कवि अब रुक नहीं सकता था। डीबीडीएन को कर्तव्य पुकार रहा था। जड़ों के पास जाकर वह उन्हें खोना नहीं चाहता था। तो भागा कवि आगे-आगे। देहाती उसके पीछे। नीचे धूल मिट्टी गड्ढे ऊपर तीखी धूप।
देहाती चिल्ला रहे थे-बकरी चोर। पकड़ों। कवि कह रहा था-आ लौट आ जड़ों की ओर आ, चल तुझे साइबर स्पेस ले चलूँ।
चोर, जड़ें और साइबर स्पेस !
समाँ बँध गया, माहौल बन गया !!
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i